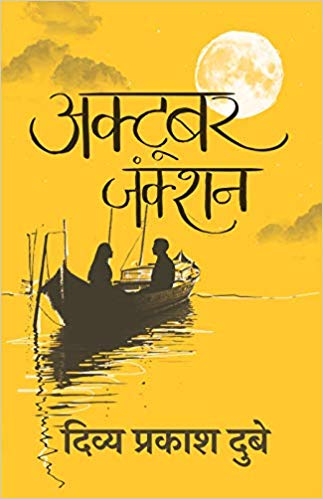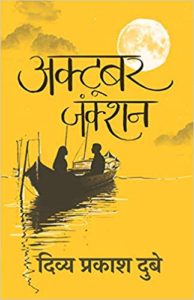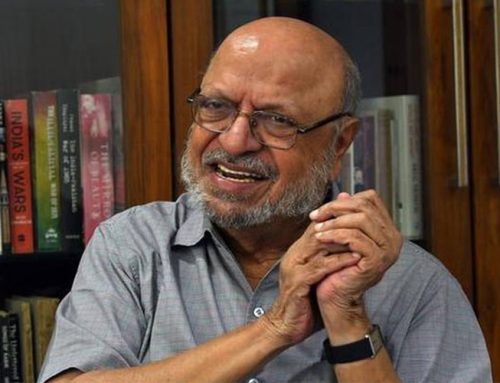पीयूष द्विवेदी
दिव्य प्रकाश दुबे का नया उपन्यास ‘अक्टूबर जंक्शन’ पढ़ते हुए यह आभास होता है कि वे ‘गुनाहों का देवता’ के खासे प्रभाव में हैं। अपने पहले उपन्यास ‘मुसाफिर कैफे’ में उन्होंने ‘गुनाहों का देवता’ के चंदर–सुधा–पम्मी जैसे पात्रों के नाम इस्तेमाल किए थे, लेकिन उनकी बुनावट एकदम नयी थी। वहीं ‘अक्टूबर जंक्शन’ में पात्रों के नाम तो नए हैं, लेकिन उनकी भावभूमि जब–तब ‘गुनाहों का देवता’ के पात्रों की याद दिलाने लगती है। दोनों ही उपन्यासों का परिवेश और परिस्थितियां एकदम जुदा हैं, लेकिन भावनात्मक धरातल पर अक्सर इनके मुख्य पात्र मूलतः एकरूप हो जाते हैं। हालांकि ‘गुनाहों का देवता’ एक सामाजिक उपन्यास है, जबकि ‘अक्टूबर जंक्शन’ की कहानी दार्शनिकता का पुट लिए हुए है।
मशहूर लेखिका चित्रा पाठक की प्रेसवार्ता से कहानी शुरू होती है, जिसमें वो अपनी प्रतिस्पर्धी लेखिका सुरभि पराशर और एक अपरिचित व्यक्ति सुदीप यादव के विषय में कुछ खुलासा करती है। फिर कहानी दस साल पहले पहुँच जाती है, जहां संघर्षरत लेखिका चित्रा पाठक और कामयाब युवा उद्यमी सुदीप यादव हमारे सामने आते हैं। 10 अक्टूबर को इन दोनों की बनारस में यूँ ही मुलाक़ात हो जाती हैं। एक–दो दिन साथ बिताने के बाद जब दोनों अपनी राह पकड़ते हैं, तो बड़े नाटकीय ढंग से ये तय कर लेते हैं कि अब वे अगले साल दस अक्टूबर को ही मिलेंगे, बीच में कोई संपर्क नहीं करेंगे। इसके बाद वे दोनों हर साल तय तारीख को मिलने लगते हैं और इसी तरह साल दर साल गुजरते हुए कहानी दस साल बाद अंत में अपने शुरूआती दृश्य पर पहुँचती है। इन दस सालों में जो भी घटनाएं होती हैं, उनमें प्रधान घटना के रूप में सुदीप–चित्रा का हर साल दस अक्टूबर को मिलना ही रहा है। हालांकि इस दौरान कोई रोमांटिक दृश्य–संवाद या अन्य कोई भी मसाला नहीं मिलता, अगर कुछ मिलता है तो बस एक नीरव उदासी। सुदीप–चित्रा की हर गतिविधि में हमें एक अव्यक्त उदासी की छाया दिखाई देती है जो कहीं–कहीं व्यक्त भी हो गयी है। यूँ भी कह सकते हैं कि उदासी इस कहानी का एक अव्यक्त किन्तु स्थायी भाव है।
दरअसल इस उपन्यास को अगर ऊपर–ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे तो हाथ कुछ नहीं आएगा। इसकी कहानी अपने में दार्शनिक विस्तार की संभावना को समेटे हुए है। कहानी की शुरुआत में जब चित्रा–सुदीप की मुलाक़ात होती है, तो चित्रा दौलत–शोहरत हासिल करने की इच्छा रखती है जबकि सुदीप इन चीजों के होने के बावजूद अपनी कम्पनी को नंबर एक बनते देखना चाहता है। यानी दोनों ही असंतुष्ट होते हैं। इसके बाद तमाम नाटकीय घटनाक्रमों से गुजरते हुए कहानी जब अंत के करीब पहुँचती है, तो चित्रा दौलत–शोहरत हासिल कर सुदीप की हालत में आ चुकी होती है और सुदीप सबकुछ गंवाकर चित्रा की स्थिति में पहुँच चुका होता है। मगर असंतोष अब भी दोनों में रहता है। यहीं एक फ़कीर आकर सुदीप को श्मशान दिखाने ले जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर विचार करें तो स्पष्ट होता है कि इसमें भारतीय ग्रंथों में वर्णित जीवन के उस सनातन दर्शन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिसमें जीवन को क्षणभंगुर मानते हुए कामना को त्याग संतोष में सुख की बात का प्रतिपादन है। यूँ ही एक बलात्कार पीड़ित लड़की को मुआवजे के रूप में कुछ हजार रुपयों के लिए पंचायती जिरह देखकर जब सुदीप को अपने खाते में जमा करोड़ों रुपये बेकार महसूस होने लगते हैं, तब धन–संग्रह के निषेध का सनातन दर्शन ही साकार होता है। ऐसे ही अनेक प्रसंग हैं जिन्हें दार्शनिक विस्तार दिया जा सकता है।
इस मजबूत दार्शनिकता के बावजूद उपन्यास कहानी की रोचकता के मामले में कमजोर पड़ जाता है। कहानी में ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं है, जो पाठकों को बांधे रख सके। सुदीप–चित्रा के लम्बे–लम्बे संवाद जिनमें दार्शनिक गहराई तो है, लेकिन एक सामान्य पाठक के लिए कोई ख़ास आकर्षण नहीं है। लिहाजा पाठकों को ये संवाद बोझिल लग सकते हैं। हालांकि लेखक ने दस साल में कहानी को बांटने का एक शिल्पगत प्रयोग किया है, लेकिन कहानी के एकदम सीधा–सपाट होने के कारण ये प्रयोग भी कोई असर नहीं छोड़ पाता। कहानी के प्रारंभ में पैदा किए कुछ रहस्यों (जैसे कि सुरभि पराशर कौन है? सुदीप यादव का क्या हुआ?) के भरोसे यदि लेखक को पाठक के अंत तक कहानी से जुड़े रहने की उम्मीद है, तो इसे ज्यादती ही कहेंगे।
भाषा की बात करें तो दिव्य प्रकाश दुबे की अंग्रेजी मिश्रित हिंदी पूर्ववत ढंग से इस उपन्यास में भी बनी रही है। आलोचनाओं के बावजूद दिव्य अपने इस भाषाई ढंग में परिवर्तन करते नहीं दिखते।
पुस्तक – अक्टूबर जंक्शन
लेखक – दिव्य प्रकाश दुबे
प्रकाशक – हिन्द युग्म
मूल्य – 125 रुपये