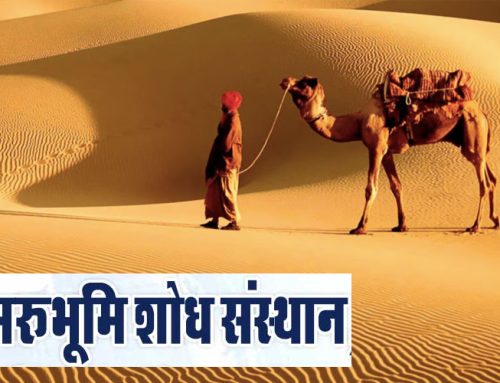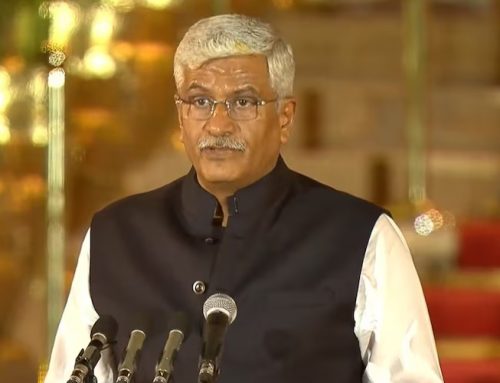हिंदी की चर्चित रचनाकार डॉ. सूर्यबाला एक बड़ी किस्सागो हैं. कथा कहने की विधा में उनकी पारंगतता का आलम यह है कि वह जब चाहती हैं, अपनी कहानियों को, उसके नायकों, पात्रों, कथानकों को एक नया व्यापक फलक दे उपन्यास का रूप दे देती हैं, बावजूद इसके उनके लिखे उपन्यासों की गिनती काफी सीमित है. वाराणसी में हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा हासिल कर वहीं अध्यापन करने वाली डॉ. सूर्यबाला की पहली कहानी साल 1972 में सारिका में प्रकाशित हुई थी, पर उनके लेखन ने गति पकड़ी साल 1975 में उनके मुंबई में बस जाने के बाद. इसी साल उनका पहला उपन्यास 'मेरे संधिपत्र' प्रकाशित हुआ. उसके बाद तो कहानी संग्रह: एक इंद्रधनुष, दिशाहीन, थाली भर चांद, मुंडेर पर, गृहप्रवेश, कात्यायनी संवाद, सांझवाती, इक्कीस कहानियां, पांच लंबी कहानियां, सिस्टर! प्लीज आप जाना नहीं, मानुष-गंध, वेणु का नया घर, प्रतिनिधि कहानियां, सूर्यबाला की प्रेम कहानियां; व्यंग्य: अजगर करे न चाकरी, धृतराष्ट्र टाइम्स, देशसेवा के अखाड़े में, भगवान ने कहा था; बाल साहित्य: झगड़ा निपटारक दफ़तर; दूरदर्शन धारावाहिक: 'पलाश के फूल', 'न, किन्नी न', 'सौदागर दुआओं के', 'एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम', 'सबको पता हैं', 'रेस' तथा' निर्वासित' आदि प्रकाशित-प्रसारित हुए. उनकी लिखी कहानी 'सज़ायाफ्ता' पर बनी टेलीफ़िल्म को पुरस्कार भी मिला. जागरण हिंदी ने उनसे उनके नए उपन्यास पर विशेष बात की, खास अंशः
– आपने काफी कुछ लिखा है, पर इतने विपुल और लोकप्रिय लेखन के बावजूद आपके उपन्यासों की गिनती काफी कम है, ऐसा क्यों?
एकदम से ऐसा नहीं है. पहले भी 'मेरे संधि पत्र', 'सुबह के इंतज़ार तक', 'अग्निपंखी', 'दीक्षांत' और 'यामिनी-कथा' नामक उपन्यास आ चुके हैं, और साहित्य जगत, आलोचकों और प्रशंसकों के बीच उसकी खूब चर्चा भी हुई. पर यह भी सच है कि इस नए उपन्यास को आने में एक लंबा वक्त तो लग ही गया.
– समकालीन कथा साहित्य में विषय पर पकड़ के मामले में सूर्यबाला का लेखन एक विशिष्ट महत्त्व रखता है, फिर भी नया उपन्यास आने में दशक भर का समय, कोई खास वजह?
वजह खास नहीं. मेरी अपनी व्यस्तताएं थीं, पर प्रकाशनों में इतना लंबा अंतराल भी नहीं रहा. मेरी रचनाएं इस बीच प्रकाशित होकर आती रही हैं, पर वह पुरानी-नई कहानियों के नए संकलनों, पुनर्प्रकाशन के रूप में थीं. मेरे ताजा उपन्यास के दो नाम हैं, 'कौन देस को वासी- वेणु की डायरी', इसे राजकमल प्रकाशन ने छापा, इस पर इससे पहले 'अलविदा अन्ना' भी तो छपा था. पर यह भी सच है कि वह उपन्यास नहीं, स्मृति-कथा था.
– तो आप मानती हैं कि आपको अपने नए उपन्यास 'कौन देस को वासी- वेणु की डायरी' को लिखने में दशक भर का समय लगा?
दशक ही क्यों, सच कहूं तो दो दशक लगे. इस उपन्यास में अलग-अलग दौर की तीन पीढ़ियां सम्मिलित हैं. जिनसे जुड़े भावों और अनुभवों को मैंने पूरे बीस साल मुंबई से अमेरिका की यात्रा और प्रवास में न केवल देखा, बल्कि जीया भी और डायरी की शक्ल में उतारती भी रही. इनमें से काफी तो अलग-अलग कथानकों के रूप में यहां-वहां छपे भी. पर तब नहीं सोचा था कि एक दिन यह एक वृहत उपन्यास के रूप में सामने आएगा.
– 'कौन देस को वासी- वेणु की डायरी' की विषय-वस्तु, पृष्ठभूमि और कथानक के बारे में कुछ बताइए?
देखिए जैसा कि मैंने कहा इसमें दो दशकों में फैला अनुभव है. जब इसकी शुरुआत हुई तो ट्रंककॉल का जमाना था. टेलीफोन बिल इतने महंगे, आज मोबाईल, ह्वाट्सएप, मैसेंजर और इंटरनेट का जमाना है. आप ऐसे समझिए कि 1992 के अमेरिका और आज के अमेरिका में प्रवासी भारतीय तो क्या खुद अमेरिकियों ने और पूरे समाज ने कितने बदलाव देखे, और उसे न केवल मैंने प्रत्यक्ष देखा, बल्कि महसूस किया. उन्हें ही मैं कागज पर उतारती गई. नोट्स बनते गए, वेणु की डायरी के ढेर सारे अंश आते गए. इन बदलावों को मैंने दो रूपों में देखा और दो नाम भी दिए, 'कौन देस को वासी' और 'वेणु की डायरी'. इसमें पश्चिम का भारतीय समाज, जीवन, परंपरा, आधुनिकता एवं उससे जुड़ी समस्या सब कुछ है.
–तो क्या यह प्रवासी भारतीयों और विस्थापन पर लिखा उपन्यास है?
कह सकते हैं. अनुभव, अनूभूति जो भी कहें. एक दौर में गांव से शहर आने वालों की विडंबना थी, आज विदेश जाने, वहीं रह जाने की विडंबना है. तीन पीढ़ियों का, उनकी संवेदनाओं से शुरू हुआ, पगा उपन्यास, जिसमें उनकी अंतर्कथा, जीवन की सार्थकता, सफलता, मनुष्यता सब शामिल है. प्रवासी भारतीय होना भारतीय समाज की महत्वाकांक्षा भी है, सपना भी और करियर भी, फिर सब कुछ मिल जाने के बाद नॉस्टेल्जिया का ड्रामा भी. लेकिन कभी-कभी वह अपने आप को, अपने परिवेश को, अपने देश और समाज को देखने की एक नई दृष्टि का मिल जाना भी होता है.अपनी ज़न्मभूमि से दूर किसी परायी धरती पर खड़े होकर वे जब अपने आप को और अपने देश को देखते हैं तो वह देखना बिलकुल अलग होता है. इस उपन्यास में अमेरिका-प्रवास में रह रहे वेणु और मेधा खुद को और अपने पीछे छूट गई जन्मभूमि को ऐसे ही देखते हैं. उन्हें अपनी मिटटी की अबोली कसक प्राय: चुभती रहती है- वे अपने परिवारजनों और उनकी स्मृतियों को सहेजे जब स्वदेश प्रत्यावृत्त होते हैं तो उनकी परिकर-परिधि में आए जन उनके रहन-सहन, आत्मविश्वास से प्रभावित होते हैं, किन्तु वेणु और मेधा के दु:ख, उदासी और अकेलापन नेपथ्य में ही रहते हैं. नई पीढ़ी की आकांक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा धनोपार्जन ही है ताकि एक बेहतर जिंदगी जी सकें, पर यह डॉलर से मिलता है क्या? इसे तो कोई अमेरिका गए प्रवासी से पूछे, जो भीतर ही भीतर कई संग्राम लड़ते रहते हैं.