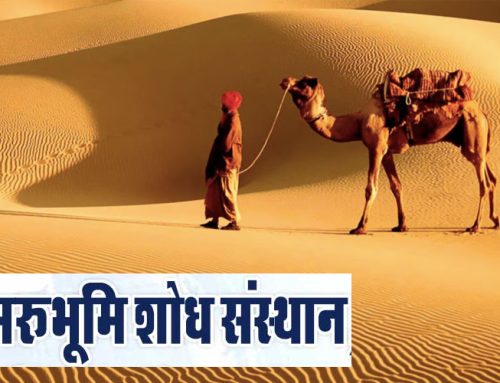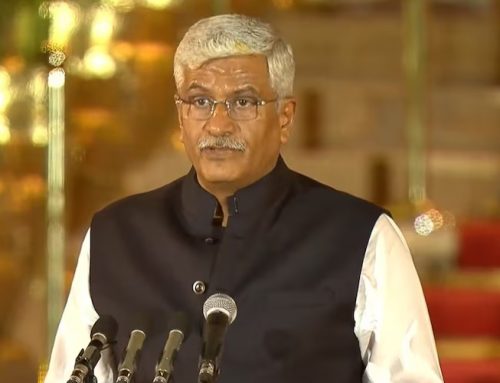राजीव रंजन प्रसाद का उपन्यास ‘लाल अंधेरा’ नक्सलवाद की समस्या के आगाज, विकास, प्रभाव, नेटवर्क आदि विविध पहलुओं को समेटता चलता है। इस उपन्यास में न केवल देश भर में व्याप्त सशस्त्र नक्सलवाद की परतों को उघाड़ा गया है, बल्कि परोक्ष ढंग से इसका समर्थन करने वाले शहरी नक्सलवाद की भी जमकर कलई खोलने का प्रयास किया गया है। कथानक की बुनावट कुछ ऐसे हुई है कि एक रौ में बहते हुए पाठक धीरे–धीरे नक्सलवाद के जंगल से नगर तक व्याप्त पूरे चक्रव्यूह को परत दर परत अपने सामने बेपर्दा पाता है। उपन्यास की कहानी कई टुकड़ों और अनेक पात्रों के बीच बिखरी हुई है। इसके अधिकांश पात्र, नक्सलवाद की समस्या के अलग–अलग पक्षों एवं किसी न किसी समाज या वर्ग विशेष के प्रतिनिधि पात्र हैं।
कहानी का सूदू नामक पात्र आजाद भारत में रजवाड़ों की व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात् बस्तर के आदिम समाज की अवस्था का एक चित्र खींचता है। बस्तर के अंतिम शासक प्रवीरचंद भंजदेव के सियासी चक्रव्यूह का शिकार होकर मारे जाने के पश्चात् खुद को उनकी प्रजा मानने वाले आदिमों की लोकतान्त्रिक भारत में क्या दशा हुई, अपना घरबार छोड़ यत्र–तत्र भागकर उन्हें किस तरह संघर्षपूर्ण जीवन बिताना पड़ा, सूदू का चरित्र आदिम समाज की इस ऐतिहासिक त्रासदी को उकेरकर रख देता है। मगर इस मुसीबत को अपनी मेहनत से धता बताकर वे जस–तस जीवन को एक लय देने में लगे रहे। लेकिन जब उन्हें लगा कि स्थिति कुछ ठीक हो रही है और उन्होंने जरा सपने देखने शुरू ही किए थे कि उनके बीच तथाकथित क्रांतिदूतों यानी नक्सलियों का आगमन हो गया। इसी तथ्य को उजागर करते हुए सूदू कहता है, ‘मैं बुधरी को बहुत प्यार किया। बहुत अच्छे से रखा। उसके दिल का सब किया। तबतक सबकुछ ठीक चलता रहा, जबतक दादा लोग हम लोग के गाँव में नहीं घुसे थे।’ यहाँ ‘दादा लोग’ का तात्पर्य नक्सलियों से ही है। सरकार की उपेक्षा के कारण पहले से ही त्रस्त आदिमों के जीवन में नक्सली अत्याचार और शोषण का कैसा अमानवीय रूप लेकर आए, उपन्यास में इसका बाखूबी चित्रण किया गया है। इसके अलावा प्रो. नीलिमा, जूही, डॉ रत्नेश, पत्रकार शिवेश, छात्र साकेत ये वो पात्र हैं, जो एक ख़ास विचारधारा से प्रभावित बौद्धिक वर्ग द्वारा बुने जाने वाले शहरी नक्सलवाद के चक्रव्यूह से रूबरू करवाते हैं।
चूंकि इस उपन्यास का जो विषय है, ऐसे विषयों की बड़ी चुनौती यह होती है कि इसमें लेखक को अनेक विचाधाराओं से जूझते हुए अपनी लेखनी की निरपेक्षता को कायम रखना पड़ता है। यह चुनौती राजीव के समक्ष भी रही होगी। लेकिन प्रशंसनीय है कि उन्होंने खुद को किसी विचारधारा के अंध–समर्थन या अंध–विरोध में उलझने से बचाते और पूर्वाग्रहों से बचते हुए प्रस्तुत विषय के साथ यथासंभव न्याय किया है। उपन्यास का ये अंश उल्लेखनीय होगा, ‘लाल हो, नीला हो या कि भगवा या कोई और रंग वैचारिक राजनीति सभी करते हैं। … लेकिन कोई भी लेफ्ट जितना आर्गनाइज्ड नहीं है। वे इंस्टिट्यूशंस पर गहरी पकड़ रखते हैं… बाकी सभी पक्ष खुद को अपने राजनीतिक साझीदार से काटकर दिखाने का प्रयास नहीं करते, लेकिन यहाँ तो वाम राजनीति भी करना है और निरपेक्षता का लेबल भी चाहिए।’ इस अंश में हम देख सकते हैं कि लेखक ने साफ़ तौर पर स्वीकारा है कि विचारधारा की राजनीति सब पक्ष करते हैं, लेकिन वे इस तथ्य को झुठला भी नहीं सकते कि आजादी के बाद ज्यादा समय तक संस्थाओं पर काबिज रहने के कारण वाम विचारधारा की इनपर बेहतर पकड़ कायम हो चुकी है। उपर्युक्त बातों से जाहिर है कि इस उपन्यास का विषय पात्रों और घटनाओं के लिहाज से न केवल व्यापक बल्कि जटिल भी है। बावजूद इसके इसे राजीव की किस्सागोई का कमाल ही कहेंगे कि ये उपन्यास पढ़ते हुए कमोबेश किसी ‘थ्रिलर’ का सा मजा आता है। इसकी जटिलता और गंभीरता के कारण बहुत अधिक ऊब की स्थिति नहीं बनती। कुल मिलाकर यह उपन्यास बन्दूक लेकर खड़े प्रत्यक्ष नक्सलियों की क्रूरता के साथ–साथ अलग–अलग बौद्धिकता के आवरण में छिपे अप्रत्यक्ष नक्सलियों के पूरे नेटवर्क को भी सामने लाता है। जो पाठक इस नक्सलवाद पर गंभीर किताबों से परहेज करते हैं, उन पाठकों को रोचक ढंग से इस विषय की व्यापक समझ प्रदान करने के लिहाज से यह उपन्यास एक महत्वपूर्ण कृति है।
– पीयूष द्विवेदी