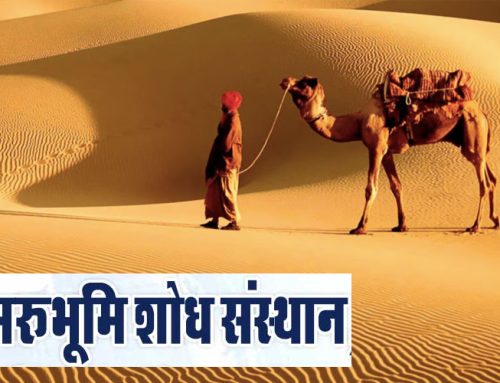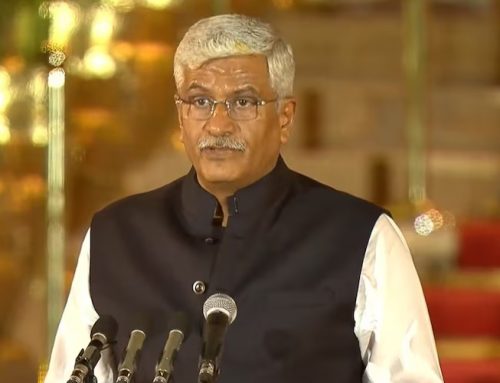समकालीन युवा कविता का प्रतिष्ठित और बहुचर्चित भारत भूषण अग्रवाल कविता पुरस्कार इस बार युवा कवि अदनान कफील दरवेश को उनकी कविता 'किबला' के लिए देने का निर्णय लिया गया है. यह कविता वागर्थ मासिक पत्रिका के सितंबर 2017 के अंक 266 में प्रकाशित हुई थी.
इस पुरस्कार की स्थापना तार-सप्तक के यशस्वी कवि भारत भूषण अग्रवाल की स्मृति में उनकी पत्नी स्वर्गीय बिन्दु अग्रवाल ने सन् 1979 में की थी. पुरस्कार समिति के निर्णायक मंडल में अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, उदय प्रकाश, अनामिका और पुरुषोत्तम अग्रवाल शामिल हैं, जो हर साल बारी-बारी से वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कविता का चयन करते हैं. इस बार के निर्णायक पुरुषोत्तम अग्रवाल थे.
युवा कवि अदनान कफील 'दरवेश' का जन्म 30 जुलाई, 1994 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गड़वार ग्राम में हुआ. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक आनर्स किया है और उनकी रचनाएं हिंदी की प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं तथा वेब ब्लॉग्स पर प्रकाशित होती रही हैं.
'किबला' के लिए अदनान कफील दरवेश को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार की संस्तुति करते हुए निर्णायक वक्तव्य में पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा कि, अदनान की यह कविता मां की दिनचर्या के आत्मीय, सहज चित्र के जरिेए 'मां और उसके जैसी तमाम औरतों' के जीवन-वास्तव को रेखांकित करती है. अपने रोजमर्रा के वास्तविक जीवन अनुभव के आधार पर गढ़े गये इस शब्द-चित्र में अदनान आस्था और उसके तंत्र यानि संगठित धर्म के बीच के संबंध की विडंबना को रेखांकित करते हैं.
अदनान की यह कविता सभ्यता, संस्कृति और धर्म में स्त्री के योगदान को, इसकी उपेक्षा को पुरजोर ढंग से रेखांकित करती है. उनकी अन्य कविताओं में भी आस-पास के जीवन, रोजमर्रा के अनुभवों को प्रभावी शब्द-संयोजन में ढालने की सामर्थ्य दिखती है.
पेश है पुरस्कृत कविता
किबला
माँ कभी मस्जिद नहीं गई
कम से कम जब से मैं जानता हूँ माँ को
हालाँकि नमाज़ पढ़ने औरतें मस्जिदें नहीं जाया करतीं हमारे यहाँ
क्यूंकि मस्जिद ख़ुदा का घर है और सिर्फ़ मर्दों की इबादतगाह
लेकिन औरतें मिन्नतें-मुरादें मांगने और ताखा भरने मस्जिदें जा सकती थीं
लेकिन माँ कभी नहीं गई
शायद उसके पास मन्नत माँगने के लिए भी समय न रहा हो
या उसकी कोई मन्नत रही ही नहीं कभी
ये कह पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है
यूँ तो माँ नइहर भी कम ही जा पाती
लेकिन रोज़ देखा है मैंने माँ को
पौ फटने के बाद से ही देर रात तक
उस अँधेरे-करियाये रसोईघर में काम करते हुए
सब कुछ करीने से सईंतते-सम्हारते-लीपते-बुहारते हुए
जहाँ उजाला भी जाने से ख़ासा कतराता था
माँ का रोज रसोईघर में काम करना
ठीक वैसा ही था जैसे सूरज का रोज निकलना
शायद किसी दिन थका-माँदा सूरज न भी निकलता
फिर भी माँ रसोईघर में सुबह-सुबह ही हाजिरी लगाती.
रोज धुएँ के बीच अँगीठी-सी दिन-रात जलती थी माँ
जिसपर पकती थीं गरम रोटियाँ और हमें निवाला नसीब होता
माँ की दुनिया में चिड़ियाँ, पहाड़, नदियाँ
अख़बार और छुट्टियाँ बिलकुल नहीं थे
उसकी दुनिया में चौका-बेलन, सूप, खरल, ओखरी और जाँता थे
जूठन से बजबजाती बाल्टी थी
जली उँगलियाँ थीं, फटी बिवाई थी
उसकी दुनिया में फूल और इत्र की खुश्बू लगभग नदारद थे
बल्कि उसके पास कभी न सूखने वाला टप्-टप् चूता पसीना था
उसकी तेज़ गंध थी
जिससे मैं माँ को अक्सर पहचानता.
ख़ाली वक़्तों में माँ चावल बीनती
और गीत गुनगुनाती-
"..लेले अईहS बालम बजरिया से चुनरी”
और हम, "कुच्छु चाहीं, कुच्छु चाहीं…" रटते रहते
और माँ डिब्बे टटोलती
कभी खोवा, कभी गुड़, कभी मलीदा
कभी मेथऊरा, कभी तिलवा और कभी जनेरे की दरी लाकर देती.
एक दिन चावल बीनते-बीनते माँ की आँखें पथरा गयीं
ज़मीन पर देर तक काम करते-करते उसके पाँव में गठिया हो गया
माँ फिर भी एक टाँग पर खटती रही
बहनों की रोज़ बढ़ती उम्र से हलकान
दिन में पाँच बार सिर पटकती ख़ुदा के सामने.
माँ के लिए दुनिया में क्यों नहीं लिखा गया अब तक कोई मर्सिया, कोई नौहा ?
मेरी माँ का ख़ुदा इतना निर्दयी क्यूँ है ?
माँ के श्रम की क़ीमत कब मिलेगी आख़िर इस दुनिया में ?
मेरी माँ की उम्र क्या कोई सरकार, किसी मुल्क का आईन वापिस कर सकता है ?
मेरी माँ के खोये स्वप्न क्या कोई उसकी आँख में
ठीक उसी जगह फिर रख सकता है जहाँ वे थे ?
माँ यूँ तो कभी मक्का नहीं गई
वो जाना चाहती थी भी या नहीं
ये कभी मैं पूछ नहीं सका
लेकिन मैं इतना भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि
माँ और उसके जैसी तमाम औरतों का क़िबला मक्के में नहीं
रसोईघर में था…